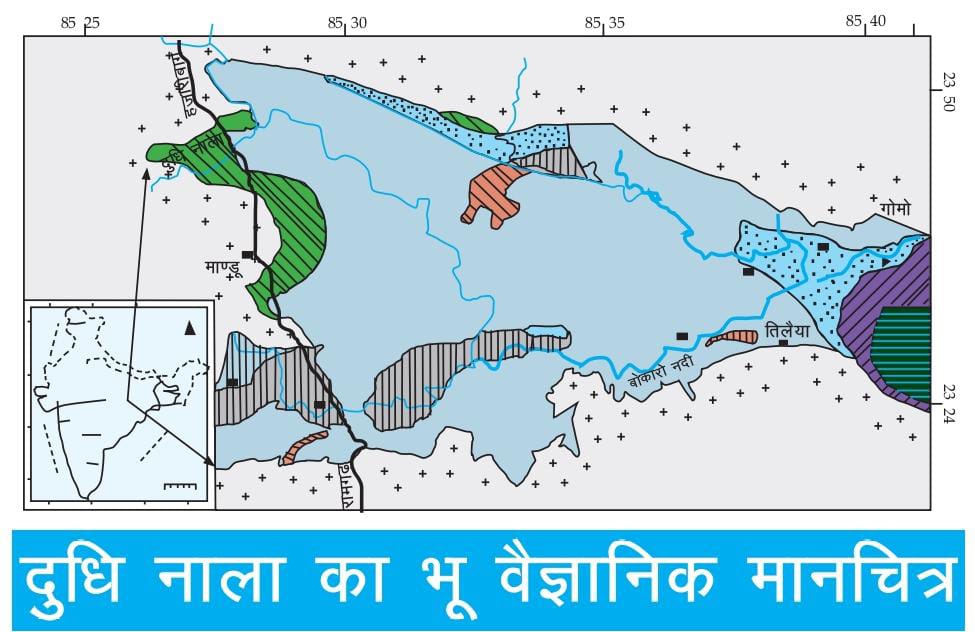-डॉ. अजय खेमरिया-
तथ्य एकः हरियाणा सरकार के 11 में से 08 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए। बीजेपी बहुमत से छह सीटें पीछे रह गयी।
तथ्य दोः महाराष्ट्र सरकार के 07 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए। बीजेपी की सीटें पहले के मुकाबले घट गयीं।
तथ्य तीनः मप्र में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 13 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव हार गए और 08 सीटें कम रहने के कारण पार्टी सत्ता से बाहर हो गयी। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार के मंत्री रहे उम्मीदवार हारे और पार्टी सत्ता से बाहर हो गयी।
इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की राज्य की सरकारों के कामकाज के परीक्षण या सोशल ऑडिट की कोई प्रमाणिक व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। मंत्री पद की अपनी एक जवाबदेही है, जिसका दलीय और सुशासन दोनों नजरिये से अपना महत्व है। पार्टी की अपेक्षा रहती है कि अतिरेक क्षमताओं वाले ये नेता न केवल खुद जीतें बल्कि आसपास भी ऐसा माहौल बनाकर रखें ताकि पार्टी उनके नाम और काम को उपलब्धि के रूप में बता सके। संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पदक्रम मंत्रिमंडल में सभी सदस्यों के बीच सिर्फ ‘प्रथम’ यानी पहले व्यक्ति का प्रावधान करता है। यानी वह मंत्रिमण्डलीय टीम का प्रथम सदस्य है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से राज्य और केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे हाथ बांधकर खड़े फॉलोअर के रूप में ढल गए हैं। देशभर में राज्यों का शासन मुख्यमंत्रियों के चेहरे और उनकी कतिपय सर्वोच्चता पर आकर टिक गया है। मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के लिये काम और अधिकार मुख्यमंत्री की दया पर ही निर्भर है। इस बीच सभी राज्यों में अफसरशाही ने सचिवालय को इतना पावरफुल बना लिया है कि मंत्रियों की अपने ही विभागों में काम कराने के लिये सांसें फूल जाती हैं।
कहने को तो मंत्री अपने विभाग का मुखिया है पर उसे अपनी योजनाओं की घोषणा करने का प्रचलित अधिकार इसलिये नहीं है क्योंकि ये काम अब मुख्यमंत्रियों ने अपने जिम्मे ले लिया है। मप्र, छतीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में पिछले 16 सालों में मंत्रियों की ताकत पूरी तरह से मुख्यमंत्रियों में समाहित हो चुकी है। जबकि होना यह चाहिये कि मंत्री खुद स्वतन्त्र होकर अपने विभाग में न केवल निर्णय लें बल्कि जनभावनाओं के अनुरूप नीतियों को लागू करें। आज स्थिति यह है कि हर विभाग में प्रमुख सचिव स्तर का आईएएस अफसर तैनात है, उसके नीचे विभाग प्रमुख भी आईएएस हैं। ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, बिजली जैसे बड़े बड़े विभागों में तो पांच आईएएस अफसर योजनाओं के अनुसार पदस्थ हैं। मसलन हर राज्य के बिजली वितरण, उत्पादन, पारेषण, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग के लिये अलग-अलग कम्पनी है और सबके मुखिया आईएएस अफसर हैं। लोक स्वास्थ्य में भी ग्रामीण मिशन, एड्स नियंत्रण, आयुष्मान के अलग-अलग आईएएस डायरेक्टर हैं। यही हाल नगरीय विकास, सड़क विकास, कृषि विभाग का है। समझा जा सकता है कि आईएएस बिरादरी की कार्य संस्कृति कैसी होती है। डॉ. राममनोहर लोहिया तो आईएएस व्यवस्था के घोर विरोधी थे और उसके स्थान पर वैकल्पिक तंत्र के समर्थक थे। सवाल यह है कि काबीना के मंत्री क्या सिर्फ मोहरे बनकर रह गए हैं और उनकी भूमिका भारत में नाममात्र की रह गई है? गहराई से विश्लेषण किया जाए तो इसके बहुआयाम है। एक तो मंत्रियों का चयन अब योग्यताओं के आधार पर नहीं जातिवर्ग, क्षेत्रीयता औऱ अलाकमान के वरहदस्त से होने लगा है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ उनकी निजी निष्ठा को तरजीह दी जाती है। बीजेपी, कांग्रेस को छोड़ बसपा, सपा, ममता, नवीन पटनायक, जगनमोहन, चंद्रशेखर जैसे सीएम तो अपनी सरकारें पूरी तरह वनमैन शो की तर्ज पर चलाते हैं।
अधिकतर सीएम अपने खास आईएएस अफसरों को इतना ताकतवर बनाकर सीएम हाउस में बिठा लेते हैं, जिनके आगे मंत्रियों की स्थिति असहाय-सी होती है। कैबिनेट की बैठकें भी आज औपचारिक होकर रह गई हैं। वहां एजेंडा सिर्फ अफसरों द्वारा पढ़ा जाता है और बगैर चर्चा के पास हो जाता है। हालत यह है कि कैबिनट बैठक का एजेंडा कुछ घण्टे पहले ही सदस्यों को दिया जाता है। जाहिर है मंत्री सिर्फ सिर हिलाकर अफसरों द्वारा बनाई गई नीतियों को मंजूर करते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब कानून या नीति के मसौदे पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होती थी। मतभेद होने पर अगली बैठक तक मामले टाले जाते थे लेकिन आज न मंत्री अध्ययन करते हैं, न उन्हें इस काम के लिये प्रेरित करने वाले नेता हैं। पूरे पांच साल निकल जाते हैं, राज्य के मंत्री सभी जिलों में जाने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। जबकि होना यह चाहिये कि हर विभाग का मंत्री मैदानी क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिये दौरा करें और जमीनी पेचीदगियां समझें। आज एक भी राज्य में मंत्री को उसके बेहतर काम के लिये नहीं जाना जाता है। राज्यों के ताकतवर मंत्री का यश उसके इलाके में हुए विकास और संकट में राजनीतिक मैनेजमेंट से मापा जाता है। डीके शिवकुमार हों या नरोत्तम मिश्रा, लोग इन्हें इसी पैमाने पर जानते हैं।
एक दूसरा पहलू मंत्रियों की क्षमता का भी है। अधिकतर इस पैमाने पर फिसड्डी होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभाग भी उनकी क्षमताओं के लिहाज से कभी नहीं देते हैं। मसलन मप्र में एमबीबीएस डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार वन मंत्री बनाये गए। राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य और जल संसाधन, पुलिस में आईजी रहे रुस्तम सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहे। कमलनाथ सरकार में दो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, दोनों ऐसे विभाग के मंत्री हैं जिनका उनकी तालीम से कोई रिश्ता नहीं है। कुल मिलाकर शैक्षणिक योग्यता को खुद मुख्यमंत्री उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में मंत्रियों को भी लगता है कि अपना गढ़ बचाए रखें और जो सुख-सुविधाएं उन्हें मिली है उनका ही दोहन कर लिया जाए। मंत्री के नाते ट्रांसफर-पोस्टिंग भर में जो उनकी बाध्यकारी भूमिका शेष रह गई है, उसी में वे अपना सम्पूर्ण कौशल झोंक देते हैं। इसीलिए ट्रांसफर को अब इंडस्ट्री कहा जाने लगा है। जिन विभागों में कम्पनी, निगम बना दिये गए हैं, वहां तो मंत्रियों को ये इंडस्ट्री चलाने का अवसर ही नहीं मिलता है। जैसे बिजली महकमे से इसे समझिए। यहां डिस्कॉम (वितरण कम्पनी) के किसी कर्मचारी या अधिकारी के ट्रांसफर की फाइल मंत्री को नहीं जाती है। आईएएस सीएमडी ही सर्वेसर्वा हैं जबकि बिजली से ही सरकारें बन और बिगड़ रही। अब सवाल यह है कि जब मंत्री केवल सुख-सुविधाओं और ट्रांसफर-पोस्टिंग तक सिमटकर रह गए हैं तो फिर इस कैबिनेट सिस्टम पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिये। वरना मौजूदा सिस्टम में तो मंत्री ऐसे ही हारते रहेंगे।
This post has already been read 14217 times!